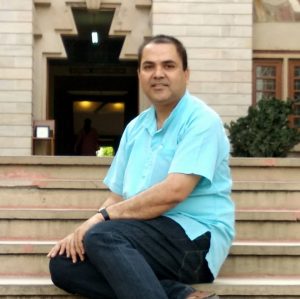
प्रेमचन्द : समाज का दर्पण और साहित्य का शिल्पी
हिंदी साहित्य की दुनिया में यदि किसी लेखक को यथार्थ का सबसे सशक्त और व्यापक चित्रकार कहा जाए तो वह मुंशी प्रेमचन्द हैं। उनकी कलम ने न केवल शब्दों को काग़ज़ पर उतारा, बल्कि उस समय के समाज की धड़कनों को पकड़कर पाठकों के सामने जीवंत कर दिया। यही कारण है कि प्रेमचन्द केवल कहानीकार या उपन्यासकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज के अंतरतम को समझने वाले दूरदर्शी चिंतक भी माने जाते हैं।
प्रेमचन्द का साहित्य हमें यह एहसास कराता है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जनजागरण और सामाजिक परिवर्तन भी है। उन्होंने अपने लेखन से यह स्थापित किया कि लेखक समाज से अलग कोई सत्ता नहीं होता, बल्कि वह समाज की विसंगतियों, पीड़ाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि होता है। प्रेमचन्द की कहानियाँ और उपन्यास आज भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनमें सामान्य जन का जीवन, उसकी संघर्षशीलता और उसकी उम्मीदें पूरी सजीवता के साथ चित्रित हुई हैं।
उनकी कहानियों में पूस की रात, ईदगाह, कफन जैसी रचनाएँ केवल घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई का साक्षात्कार कराती हैं। होरी और धनिया जैसे पात्र भारतीय कृषक जीवन के यथार्थ को सामने लाते हैं, तो गोदान आज भी किसान की दुर्दशा का शाश्वत आख्यान प्रतीत होता है। प्रेमचन्द ने दिखाया कि साहित्य का केंद्रबिंदु महल की रंगीनियाँ नहीं, बल्कि खेतों की मेड़, झोंपड़ी की चूल्हा-धुआँ और मेहनतकश जनता का जीवन है।
उनकी लेखनी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और विषमताओं पर तीखा प्रहार किया। सामंती शोषण, वर्ग-विभाजन, स्त्रियों की दयनीय स्थिति और गरीबों की बदहाली उनके साहित्य का मूल स्वर है। उन्होंने किसी सैद्धांतिक मंच से उपदेश नहीं दिए, बल्कि जीवन की घटनाओं के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयाँ सामने रखीं। यही उनकी ताक़त है—वह उपदेशक नहीं, बल्कि सृजनात्मक मार्गदर्शक हैं।
प्रेमचन्द का महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने भारतीय साहित्य को पश्चिमी यथार्थवाद के प्रभाव से आगे बढ़ाकर अपनी मिट्टी में जड़ें जमाई। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। न तो उसमें कृत्रिमता है और न ही बनावट। उनकी रचनाओं को पढ़कर लगता है कि जैसे गाँव का कोई बुजुर्ग या किसान अपने अनुभव साझा कर रहा हो। यही भाषा-पद्धति प्रेमचन्द को जन-जन तक पहुँचाने में सहायक बनी।
आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रेमचन्द हमारे लिए प्रासंगिक क्यों हैं? उत्तर स्पष्ट है—क्योंकि समाज की अनेक विसंगतियाँ अभी भी वैसी ही हैं जैसी प्रेमचन्द के दौर में थीं। किसान आज भी संकटग्रस्त है, श्रमिक आज भी असुरक्षित है, स्त्रियाँ आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं और गरीब आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर है। प्रेमचन्द का साहित्य हमें यह चेतावनी देता है कि जब तक समाज में शोषण और असमानता है, तब तक उनकी रचनाएँ हमें आईना दिखाती रहेंगी।
प्रेमचन्द की सबसे बड़ी विरासत उनकी मानवीय दृष्टि है। उन्होंने साहित्य को राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति से जोड़ा, परंतु उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा मनुष्य की गरिमा की रक्षा रहा। उनका विश्वास था कि साहित्य का मूल्य उसी में है जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे। यही कारण है कि वे केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, बल्कि भारतीय सामाजिक चेतना के भी मार्गदर्शक बन गए।
प्रेमचन्द : समाज का दर्पण और साहित्य का शिल्पी
हिंदी साहित्य की दुनिया में यदि किसी लेखक को यथार्थ का सबसे सशक्त और व्यापक चित्रकार कहा जाए तो वह मुंशी प्रेमचन्द हैं। उनकी कलम ने न केवल शब्दों को काग़ज़ पर उतारा, बल्कि उस समय के समाज की धड़कनों को पकड़कर पाठकों के सामने जीवंत कर दिया। यही कारण है कि प्रेमचन्द केवल कहानीकार या उपन्यासकार नहीं, बल्कि भारतीय समाज के अंतरतम को समझने वाले दूरदर्शी चिंतक भी माने जाते हैं।
प्रेमचन्द का साहित्य हमें यह एहसास कराता है कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जनजागरण और सामाजिक परिवर्तन भी है। उन्होंने अपने लेखन से यह स्थापित किया कि लेखक समाज से अलग कोई सत्ता नहीं होता, बल्कि वह समाज की विसंगतियों, पीड़ाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि होता है। प्रेमचन्द की कहानियाँ और उपन्यास आज भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि उनमें सामान्य जन का जीवन, उसकी संघर्षशीलता और उसकी उम्मीदें पूरी सजीवता के साथ चित्रित हुई हैं।
उनकी कहानियों में पूस की रात, ईदगाह, कफन जैसी रचनाएँ केवल घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की गहराई का साक्षात्कार कराती हैं। होरी और धनिया जैसे पात्र भारतीय कृषक जीवन के यथार्थ को सामने लाते हैं, तो गोदान आज भी किसान की दुर्दशा का शाश्वत आख्यान प्रतीत होता है। प्रेमचन्द ने दिखाया कि साहित्य का केंद्रबिंदु महल की रंगीनियाँ नहीं, बल्कि खेतों की मेड़, झोंपड़ी की चूल्हा-धुआँ और मेहनतकश जनता का जीवन है।
उनकी लेखनी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और विषमताओं पर तीखा प्रहार किया। सामंती शोषण, वर्ग-विभाजन, स्त्रियों की दयनीय स्थिति और गरीबों की बदहाली उनके साहित्य का मूल स्वर है। उन्होंने किसी सैद्धांतिक मंच से उपदेश नहीं दिए, बल्कि जीवन की घटनाओं के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाइयाँ सामने रखीं। यही उनकी ताक़त है—वह उपदेशक नहीं, बल्कि सृजनात्मक मार्गदर्शक हैं।
प्रेमचन्द का महत्व इस बात में भी है कि उन्होंने भारतीय साहित्य को पश्चिमी यथार्थवाद के प्रभाव से आगे बढ़ाकर अपनी मिट्टी में जड़ें जमाई। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की है। न तो उसमें कृत्रिमता है और न ही बनावट। उनकी रचनाओं को पढ़कर लगता है कि जैसे गाँव का कोई बुजुर्ग या किसान अपने अनुभव साझा कर रहा हो। यही भाषा-पद्धति प्रेमचन्द को जन-जन तक पहुँचाने में सहायक बनी।
आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रेमचन्द हमारे लिए प्रासंगिक क्यों हैं? उत्तर स्पष्ट है—क्योंकि समाज की अनेक विसंगतियाँ अभी भी वैसी ही हैं जैसी प्रेमचन्द के दौर में थीं। किसान आज भी संकटग्रस्त है, श्रमिक आज भी असुरक्षित है, स्त्रियाँ आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं और गरीब आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर है। प्रेमचन्द का साहित्य हमें यह चेतावनी देता है कि जब तक समाज में शोषण और असमानता है, तब तक उनकी रचनाएँ हमें आईना दिखाती रहेंगी।
प्रेमचन्द की सबसे बड़ी विरासत उनकी मानवीय दृष्टि है। उन्होंने साहित्य को राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति से जोड़ा, परंतु उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा मनुष्य की गरिमा की रक्षा रहा। उनका विश्वास था कि साहित्य का मूल्य उसी में है जो समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे। यही कारण है कि वे केवल हिंदी साहित्य के ही नहीं, बल्कि भारतीय सामाजिक चेतना के भी मार्गदर्शक बन गए।
इस विशेषांक के माध्यम से हम प्रेमचन्द को केवल एक साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि उस युगनिर्माता विचारक के रूप में स्मरण कर रहे हैं जिसने अपनी कलम से करोड़ों दिलों में संवेदना, करुणा और न्याय की आकांक्षा जगाई। प्रेमचन्द आज भी हमारे बीच जीवित हैं—हर उस कहानी में जो शोषितों की पीड़ा कहती है, हर उस उपन्यास में जो समाज की विसंगतियों पर सवाल उठाता है, और हर उस पाठक में जो उनकी रचनाओं से न्यायपूर्ण समाज का सपना देखता है।
इस अंक के संपादन में प्रो. पंढरी नाथ पाटील, डॉ. श्रुति गौतम , डॉ. अनुराग सिंह, अमित, उज्ज्वल, हर्षित, श्रद्धा और शिवम के साथ जिन्होंने भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मदद की है उनका विशेष धन्यवाद देता हूँ। साथ ही इस विशेषांक को आने में काफी विलंब हुआ है उसके लिए पाठकों से माफी…. और कोई त्रुटि रह गई हो तो आगे से सहचर टीम कोशिश करेगी की यथासंभव त्रुटि कम हो…. साथ ही सभी लेखकों का धन्यवाद जिन्होंने इस विशेषांक के लिए अपना शोधालेख और अन्य कॉलम के लिए अपनी मौलिक रचनाएँ हमें भेजी…. आगे भी आप सभी लेखकों से ऐसे ही सहयोग की आशा। अंत में यह अंक आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।




 Views This Month : 2860
Views This Month : 2860 Total views : 906331
Total views : 906331