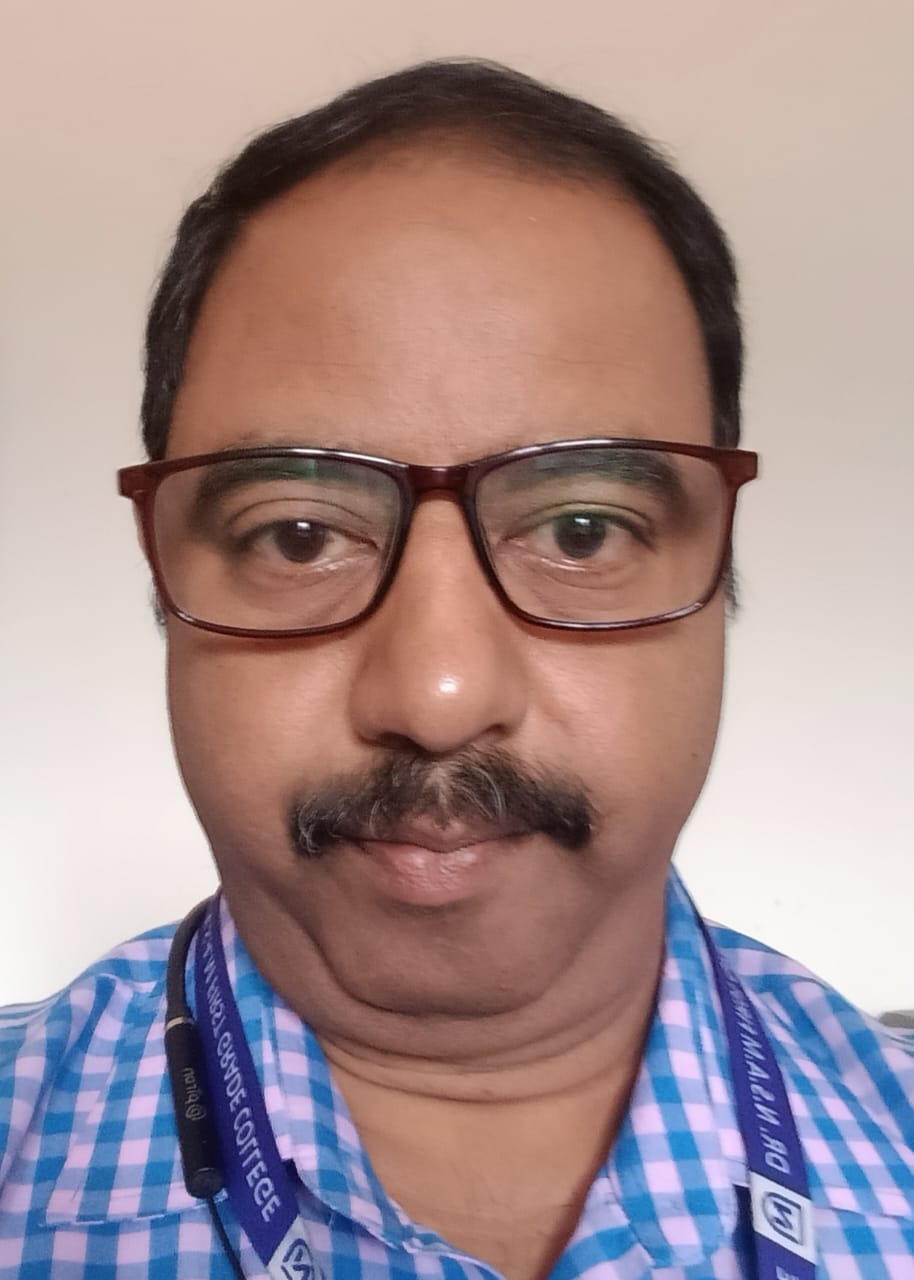
शोध सार:
मुंशी प्रेमचंद का गोदान हिंदी साहित्य की कालजयी कृति मानी जाती है| यह एक सामाजिक दर्पण है, जो औपनिवेशिक भारत के किसानों के शोषण, वर्ग संघर्ष और परंपरागत मूल्यों की उलझनों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। होरी, इस उपन्यास का नायक है | वह कर्तव्यनिष्ठ किसान है और साथ में सामाजिक अन्याय का शिकार और मानसिक द्वंद्व का प्रतीक भी है |
यह शोधपत्र होरी के मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर केंद्रित है। उसके भीतर चल रही मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल ही उसका संघर्ष है | एक ओर सामाजिक नैतिकता है, दूसरी ओर वह मानसिक संघर्ष जो समय के साथ परत दर परत उभरता है। यह शोध यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि होरी का व्यक्तित्व केवल आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का निष्कर्ष नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सजीव चित्रण भी है जो उसे एक जटिल और त्रासदीपूर्ण चरित्र बना देता है |
इस अध्ययन में होरी के चरित्र का विश्लेषण फ्रायड का मनोविश्लेषण, स्किनर का व्यवहारवाद, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, जंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, सेलिगम और मेयर का सीखा हुआ असहायपन एवं फेस्तिंग का संज्ञानात्मक असंगति जैसे सिद्धांतों के आलोक में किया गया है।
प्रस्तावना :
साहित्य केवल समाज का चित्र नहीं, बल्कि मानव मन की गहराइयों का विवेचन भी है। सिगमंड फ्रायड, कार्ल जंग जैसे मनोविश्लेषकों का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार केवल बाह्य परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अवचेतन मन, दबी इच्छाओं और आंतरिक द्वंद्वों का परिणाम है। मनोविश्लेषकों का यही दृष्टिकोण साहित्यिक पात्रों को मनोवैज्ञानिक अध्ययन के दायरे में ला खडा कर देता है|
प्रेमचंद का ‘गोदान’ भारतीय ग्रामीण जीवन की जटिलताओं का सजीव दस्तावेज है, जिसमें नायक होरी एक सामान्य किसान होते हुए भी असाधारण मनोवैज्ञानिक गहराई का वहन करता है।
इस शोधपत्र में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों के आधार पर होरी के चरित्र का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है| इसमें सिगमंड फ्रायड का ‘मनोविश्लेषण सिद्धांत’ (इदम्, अहम्, पराहम्), मार्टिन सेलिगम और स्टीवन एफ. मेयर का ‘सीखी हुई असहायता का सिद्धांत’, बी.एफ. स्किनर का ‘व्यवहारवाद’, अब्राहम मैस्लो का ‘आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत’, कार्ल जंग का ‘विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान’, लियोन फेस्टिंगर का ‘संज्ञानात्मक असंगति’ जैसे सिद्धांतों को आधार बनाया गया है | यह विश्लेषण यह दिखाने का प्रयास करता है कि होरी का संघर्ष गहरा मनोवैज्ञानिक है, जो उसे एक जटिल और त्रासदीपूर्ण चरित्र बना देता है |
- सिग्मंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के आलोक में होरी
सिगमंड फ्रायड का ‘मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत’[1] मानव मन की संरचना और व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मनुष्य के व्यवहार की गहराइयों को समझने के लिए सिग्मंड फ्रायड ने मानसिक संरचना को तीन स्तरों में विभाजित किया — इदम्[2], अहम्[3], पराहम्[4] । यह संरचना व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं, सामाजिक मानकों और यथार्थबोध के मध्य संतुलन स्थापित करती है |
- इदम् – यह वह मानसिक तत्व है, जो बिना किसी सामाजिक या नैतिक प्रतिबंध के तत्काल संतुष्टि या सुख की लालसा रखता है। यह व्यक्ति की मूलभूत इच्छाओं और प्रवृत्तियों का स्रोत है, जो आनंद सिद्धांत[5] पर कार्य करता है|
- अहम् – वास्तविकता सिद्धांत[6] के आधार पर कार्य करता है, जो इदम् की इच्छाओं और बाहरी दुनिया के वास्तविक स्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह तर्कसंगत सोच और सामाजिक सीमाओं के भीतर इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है।
- पराहम् – नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उसे सही-गलत का बोध कराता है |
1.1 होरी के व्यक्तित्व में इदम् की भूमिका:
होरी के भीतर इदम् की प्रवृत्ति उसे तात्कालिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लालायित करती है, विशेष रूप से गाय खरीदने की अपेक्षा में। आर्थिक असमर्थता के बावजूद वह कर्ज़ लेकर गाय खरीदलेने के लिए तैयार हो जाता है |
फ्रायड के अनुसार, हमारे विचारों और भावनाओं का एक बड़ा भाग अचेतन मन[7] में रहता है, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। होरी के अवचेतन ने गाय को धार्मिक सम्मान और सामाजिक स्वीकृति के प्रतीक के रूप में मान लिया है। आर्थिक विवशता एवं यथार्थ स्थितियों से परिचित होते हुए भी, उसके अवचेतन मन में छिपी इच्छा तर्क को पीछे छोड़ देती है। इदम् की प्रधानता होरी के पारिवारिक जीवन में असंतोलन, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव जैसे स्थितियों को जन्म देता हुआ दृष्टिगोचर होता है |
1.2 होरी के व्यक्तित्व में अहम् की भूमिका :
अहम् का कार्य इदम् की इच्छाओं को वास्तविकता और व्यवहारिकता के अनुसार संतुलित करना होता है। होरी जब गाय खरीदने की बात रखता है तब धनिया विरोध करती है | होरी एक क्षण के लिए अहम् के प्रभाव में आकर अपने निर्णय पर पुनर्विचार तो करता है, लेकिन अंततः इदम् उस पर इतना जोर डालता है कि वास्तविकता की अनदेखी कर हठपूर्वक गाय को खरीद ही लेता है |
होरी इदम् की इच्छा को अहम् के माध्यम से तर्क देकर सही ठहराने की कोशिश करता है | होरी के इदम् के लिए गाय धार्मिक प्रतीक है और उसे पालना सामाजिक प्रतिष्ठा है | होरी का अहम् उसे गाय खरीदने के बाद की परिस्थितियों से जूझने और समाधान खोजने को प्रेरित करता है।
1.3 होरी के व्यक्तित्व में पराहम् की भूमिका:
होरी के व्यक्तित्व में पराहम् की भूमिका उसकी नैतिक प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा तथा सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के प्रति आस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वह अपने निर्णयों में निजी सुख-सुविधा को तिलांजलि देकर समाज, परिवार और धर्म के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सर्वोच्च मानता है।
गाय के प्रति उसकी भावनात्मक लगाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी हुई है| आर्थिक दुःस्थिति के बावजूद वह इसे सामाजिक मर्यादा की पूर्ति के रूप में देखता है, जो पराहम् की ही प्रेरणा है।
झुनिया के मामले में, जब पूरा गाँव उसके विरुद्ध खड़ा होता है, तब भी वह कहता है — “ वहाँ तो उनके दोनों लड़के ख़ून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक़ आदमी मिला, उसकी बांह पकड़कर दग़ा दे गया। मैं भी निकाल दूँगा, तो इस दशा में वह कहीं मेहनत – मजूरी भी तो न कर सकेगी। कहीं डूब-धस मरी तो किसे अपराध लगेगा। रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक है | लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रहीं। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम रहीं कर सकता।”[8] यह न केवल उसकी करुणा को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार के भय के बावजूद जो निर्णय वह लेता है, उसमें उसकी नैतिक दृढ़ता भी परिलक्षित होती है।
इसके अतिरिक्त, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह गोदान करता है—एक ऐसा त्याग जो उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति की भावना से प्रेरित होता है।
इस प्रकार होरी का पराहम् उसे जीवनभर मर्यादा, कर्तव्य और त्याग के मार्ग पर बनाए रखता है—जिससे वह केवल एक साधारण किसान नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों का प्रतीक बनकर सामने आता है।
- मार्टिन सेलिगम और स्टीवन एफ. मेयर की ‘सीखी हुई असहायता’ का सिद्धांत [9](1967):
सीखी हुई असहायता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति लगातार असफलताओं के कारण यह मान लेता है कि अब उसके प्रयास व्यर्थ हैं, और इस मनास्थिति के चलते वह समस्याओं से निपटने की कोशिश करना छोड़ देता है | इस कारण वह निष्क्रिय और भाग्यवादी बन जाता है|
सीखी हुई असहायता सिद्धांत के अनुसार, होरी लगातार असफलताओं के कारण बदलाव का प्रयास छोड़ देता है। गोबर जब यह पूछता है कि हर रोज़ मालिकों की चापलूसी क्यों करना, जब कि सारा बोझ उन्हीं को उठाना पड़ता है? फिर किसी को सलाम करने की ज़रूरत ही क्या! होरी कहता है – सलामी करने न जाएं , तो रहें कहा ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है, तो अपना क्या बस है?[10] यह संवाद होरी की भाग्यवादिता और निष्क्रियता को दर्शाता है, जहाँ वह अपने हालात को बदलने की बजाय उन्हें नियति मानकर स्वीकार कर लेता है |
बी.एफ. स्किनर का व्यवहारवाद और होरी:
बी.एफ. स्किनर का व्यवहारवाद यह कहता है कि मनुष्य का व्यवहार बाहरी परिस्थितियों और सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है, यह समय, समाज और परिस्थिति के अनुसार हर क्षण नया आकार लेती है।
होरी के व्यक्तित्व के कई स्थानों पर व्यवहारवाद की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है | होरी सामाजिक दबावों और सम्मान की लालसा में निर्णय लेता है, न कि स्वतंत्र सोच से। वह समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीने की तीव्र इच्छा रखता है | गाय होरी के लिए सामाजिक सम्मान का प्रतीक है, और वह आर्थिक तंगी के बावजूद उसे पालने के लिए आतुर रहता है|
होरी का व्यवहार भय और दंड से बचने की प्रवृत्ति से भी संचालित है। वह ज़मींदार की खुशामद करता है ताकि बेदखली या कुड़की से बच सके। वह कहता है –
“गाँव में इतने आदमी तो हैं किस पर बेदखली नहीं आयी, किस पर कुड़की नहीं आयी| जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है| तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है।”[11]
इन उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि होरी का व्यवहार स्किनर के व्यवहारवाद की पुष्टि करता है, जिसमें व्यक्ति के निर्णय स्वतंत्र इच्छा से नहीं, बल्कि सामाजिक दबावों, पुरस्कारों की इच्छा और दंड की आशंका से संचालित होते हैं |
- एब्राहम मैस्लो का ‘आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत’-
मानव जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, परंतु उसकी प्राथमिकताएँ परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एब्राहम मैस्लो ने इस जटिल विषय को गहराई से समझने के लिए “आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत” प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि मानव की आवश्यकताएँ एक निश्चित क्रम में विकसित होती हैं और जब तक एक स्तर की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती, व्यक्ति अगले स्तर की ओर अग्रसर नहीं हो सकता।
आवश्यकता के पाँच स्तर:
1.शारीरिक आवश्यकताएँ [12] – भोजन, पानी, वायु, आवास, नींद जैसे मूलभूत जीवन-निर्वाह के साधन
- सुरक्षा आवश्यकताएँ [13] – सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता व्यवस्था की भावना
- प्रेम और संबंध[14] – मित्रता, परिवार, सामाजिक जुड़ाव एवं अपनापन की भावना
- आत्म-सम्मान की आवश्यकता[15] – आत्म-आदर, मान्यता, सफलता व स्वतंत्रता जैसे पहलुओं की पूर्ति
- आत्मसाक्षात्कार[16] – स्वयं की पूर्णता की और यात्रा, समस्या समाधान, आत्म-विकास आदि
होरी इस सिद्धांत का सजीव उदाहरण है। आरंभ में वह एक किसान के रूप में भोजन, जल, आवास और कृषि संसाधनों जैसी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। इसके बाद, परिवार को सुरक्षित रखने और कर्ज़ से बचने का प्रयास उसकी सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, होरी सामाजिक स्वीकृति की आकांक्षा में गाय खरीदने का निर्णय लेता है, जो उसकी प्रतिष्ठा की भावना से जुड़ा है। उसके लिए “इज्जत से जीना” केवल आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक अस्तित्व की शर्त बन जाता है। यह दर्शाता है कि सम्मान की आवश्यकता उसके निर्णयों को कितना प्रभावित करती है।
झुनिया को अपनाना और अपने जीवन के अंत में गोदान करना, सारे सामाजिक दबावों के बावजूद नैतिक विकल्प चुनना है – यह उसके आत्म-साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को इंगित करता है—जहाँ वह अपने अस्तित्व को त्याग, करुणा और धर्म के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार, होरी की जीवन यात्रा मैस्लो के पाँचों स्तरों को स्पर्श करती है।
कार्ल जंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ;
मानव व्यक्तित्व की गहराइयों को समझने के लिए स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जंग ने अपने ‘विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान’ में यह माना कि व्यक्ति का व्यवहार केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अचेतन मन,[17] व्यक्त,[18] छाया,[19] सामूहिक अचेतन[20] और आत्मबोध[21] की प्रक्रिया से भी प्रभावित होता है।
अंतर्मुखता और भावना-प्रधान व्यक्तित्व ;
कार्ल जंग के अनुसार, अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर की दुनिया में जीता है और गहरी नैतिक चेतना रखता है। गोदान का नायक होरी इसी व्यक्तित्व का प्रतीक है | वह समाज का विरोध नहीं करता, संघर्षों को मौन रूप से सहता है और भावनाओं व कर्तव्यबोध के आधार पर निर्णय लेता है।
गो हत्या के मामले में जब पुलिस हीरा के घर की तलाशी लेने की बात कहती है तो – “होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था, जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो| तलाशी उसके घर हुई तो, उसके भाई के घर हुई तो, एक ही बात है। हीरा अलग सही; पर दुनिया तो जानती है, वह उसका भाई है; मगर इस वक़्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते, तो इसी वक़्त पचास रुपए लाकर दारोग़ाजी के चरणों पर रख देता और कहता – सरकार, मेरी इज़्ज़त अब आपके हाथ है।”[22] तो यह उसके आत्म-सम्मान और नैतिक पूँजी की भावना को दर्शाता है।
- व्यक्त:
‘व्यक्त’ वह मुखौटा है जो व्यक्ति समाज के सामने पहनता है। होरी समाज में एक प्रतिष्ठित छवि बनाए रखने के लिए अपने भीतर के संघर्षों को छिपाता है। वह गोबर के अपराध को छिपाता है, हीरा के अन्याय को सहता है — केवल इसलिए कि उसकी इज्जतदार छवि बनी रहे |
- छाया:
‘छाया’ वह दबा हुआ पक्ष है जिसे व्यक्ति समाज के डर से स्वीकार नहीं करता, पर जो उसके निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। गोदान में होरी की छाया में उसका दब्बूपन, आत्म-त्याग और झूठ शामिल हैं। वह यह मानता है कि हीरा ने जो किया, वह गलत था… पर अब पुलिस आएगी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी| तो यह स्पष्ट होता है कि वह सत्य को जानते हुए भी डर और सामाजिक अस्वीकृति के भय से उसे छिपाता है। उसकी छाया उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करती है जो उसके मूल स्वभाव से मेल नहीं खाते, पर सामाजिक छवि बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाते हैं |
कार्ल जंग के आत्मबोध सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति तब पूर्ण होता है जब वह अपने चेतन और अचेतन पक्षों—विशेषकर व्यक्त और छाया — को स्वीकार कर उन्हें एकीकृत करता है। यह केवल मानसिक परिपक्वता नहीं, बल्कि आत्म-स्वीकृति और स्वतंत्र पहचान प्राप्त करने की प्रक्रिया है।
प्रेमचंद के गोदान का नायक होरी इस आत्मबोध की यात्रा में एक संघर्षशील किंतु अधूरा पात्र है। उसका संपूर्ण जीवन सामाजिक अपेक्षाओं को निभाने में व्यतीत होता है—वह परिवार, जाति और परंपरा के दायरे में ऐसा उलझा रहता है कि स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं करता।
होरी का अंतिम कार्य गोदान प्रतीकात्मक रूप से त्याग का चरम है, परंतु यह निर्णय भी सामाजिक मर्यादाओं के दबाव में लिया गया है, न कि आत्मबोध की चेतना से प्रेरित होकर।
होरी अपने व्यक्त को बनाए रखने के लिए छाया पक्ष—जैसे डर, झूठ और आत्मग्लानि—को भीतर दबाता है। वह सही-गलत जानता है, फिर भी सामाजिक छवि बनाए रखने के लिए सत्य को छिपाता है। इस प्रकार, वह अपने व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाता — जो आत्मबोध के लिए अनिवार्य है।
लियोन फेस्टिंगर का सिद्धांत संज्ञानात्मक असंगति (1957)
मनोविज्ञानी लियोन फेस्टिंगर का संज्ञानात्मक असंगति [23] सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि जब व्यक्ति के विचार, विश्वास और व्यवहार आपस में विरोधाभासी होते हैं, तो वह मानसिक तनाव (dissonance) का अनुभव करता है। इस तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति या तो अपनी धारणाओं में परिवर्तन करता है, या फिर अपने विरोधाभासी व्यवहार को तर्कसंगत ठहराने के लिए नए औचित्य खोजने लगता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति के निर्णयों और मानसिक संरचना को गहराई से प्रभावित करती है।
निर्धनता के बावजूद होरी गाय को न केवल पारिवारिक उपयोग, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक पुण्य का स्रोत मानता है।
होरी अपने परिवार की भलाई के लिए सदैव सजग रहता है—धनिया के कष्ट और गोबर के भविष्य की चिंता उसके भीतर स्पष्ट दिखती है। लेकिन जब यही परिवार उसके निर्णयों का विरोध करता है, तो वह सामाजिक दृष्टि से उपहास का भय जताता है | उसके व्यवहार में व्यावहारिक आवश्यकताओं से अधिक समाज की नजरों का डर और मान्यता पाने की लालसा काम कर रही है।
यह संज्ञानात्मक द्वंद्व उसके समूचे जीवन पर हावी रहता है—व्यवहारिक विवेक और सामाजिक आदर्शों के बीच। वह बार-बार अपने निर्णयों को धार्मिक पुण्य, आत्म-संयम और प्रतिष्ठा के तर्कों से उचित ठहराने का प्रयास करता है, भले ही उनके परिणाम दुखद ही क्यों न हों। वह अपनी असमर्थताओं को आदर्शों की आड़ में छिपाकर उन्हें स्वीकार्य और उच्चतर सिद्ध करने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास करता है।
अंततः, जब वह मृत्यु के निकट होता है, तो गोदान करके वह अपनी मानसिक असंगति का समाधान खोजता है। गाय का दान न केवल धार्मिक अनुश्रुति का द्योतक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि होरी अंत तक सामाजिक मान्यताओं के अधीन अपनी पहचान और मुक्ति को परिभाषित करता है।
इस तरह दृष्टव्य है कि संज्ञानात्मक असंगति के आलोक में होरी का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कथा बन जाती है, जो परंपराओं, आस्थाओं और सामाजिक स्वीकृति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते-करते आत्मविरोध और त्रासदी का शिकार हो जाता है।
निष्कर्ष
प्रेमचंद का गोदान केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं, बल्कि गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध उपन्यास है। होरी के व्यक्तित्व की बनावट केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, अपितु उसके भीतर दबी इच्छाओं, नैतिक दायित्वों, सामाजिक दबावों, आत्मसम्मान और आत्मवंचना का परिणाम भी है | उसका व्यवहार भावनाओं, भय, मर्यादा और सामाजिक अपेक्षाओं के टकराव से उत्पन्न मानसिक द्वंद्वों का प्रतिबिंब है। इसी जटिलता में गोदान की मनोवैज्ञानिक गहराई निहित है, जो इसे केवल एक सामाजिक उपन्यास नहीं, बल्कि मानसिक संरचना का भी यथार्थचित्र बनाती है।
उपन्यास में होरी एक ऐसा पात्र बन जाता है, जो न केवल भारतीय ग्रामीण समाज की विडंबनाओं का प्रतिनिधि है, बल्कि मानव मन की गहराइयों, आंतरिक असंतुलन और अधूरी आत्मबोध-यात्रा का भी प्रतीक है—जो गोदान को केवल साहित्यिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कालजयी कृति बना देता है
संदर्भ ग्रंथ
- ‘गोदान’(उपन्यास) प्रेमचंद; विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, 2013
- A General Introduction to Psychoanalysis by Sigmund Freud: Publisher : CreateSpace Independent Publishing Platform; September 2017
- A Theory of Human Motivation by Abraham H Maslow, Publisher: bnpublishing.com January 2017
- Science And Human Behavior by F Skinner Publisher : Free Press, 1965
- The Archetypes and the Collective Unconscious , G. Jung: Publisher : Princeton University Press,1959
[1] Psychoanalytic Theory
[2] Id
[3] Ego
[4] Superego
[5] Pleasure Principle
[6] Reality Principle
[7] Unconscious Mind
[8] गोदान’(उपन्यास) प्रेमचंद; विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, 2013, पृष्ट संख्या 115
[9] Learned Helplessness
[10] गोदान’(उपन्यास) प्रेमचंद; विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, 2013, पृष्ट संख्या 16
[11] गोदान’(उपन्यास) प्रेमचंद; विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, 2013, पृष्ट संख्या 5
[12] Physiological Needs
[13] Safety Needs
[14] Love and Belongingness
[15] Esteem Needs
[16] Self-Actualization
[17] Unconscious mind
[18] Persona
[19] Shadow
[20] Collective Unconscious
[21] Individuation
[22] गोदान’(उपन्यास) प्रेमचंद; विश्वभारती प्रकाशन, सीताबर्डी, नागपुर, 2013, पृष्ट संख्या 103
[23] Cognitive Dissonance
डॉ. सुनील बसवाराजा मलगी
सह प्राध्यापक
डॉ एन एस ए एम् फर्स्ट ग्रेड कालेज
निट्टे मानद विश्वविद्यालय




 Views This Month : 2860
Views This Month : 2860 Total views : 906331
Total views : 906331